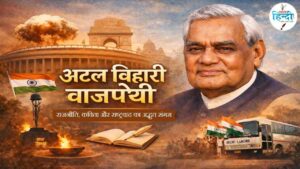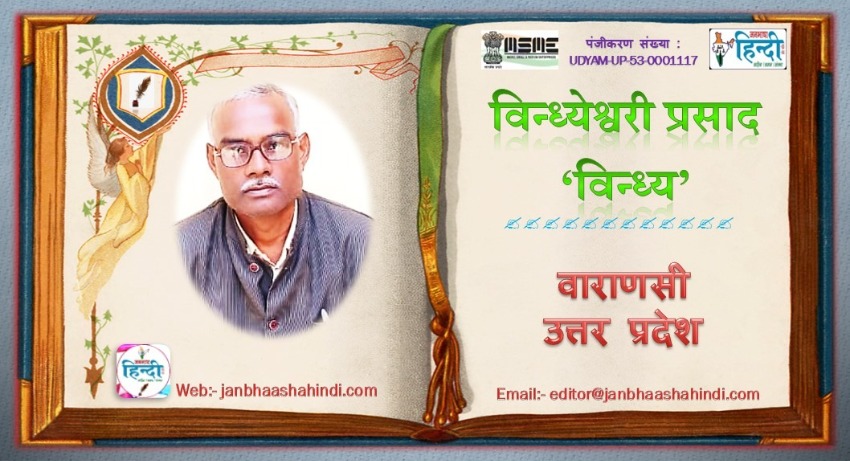
विन्ध्येश्वरी प्रसाद
Table of Contents
दास्ताने जिन्दगी

दास्ताने जिन्दगी
बादलों की छाँव-सी है, दास्ताने-जिन्दगी।
आ गयी है हम सभी को, आजमाने-जिन्दगी।
फूल खिलते हैं तनिक, काँटो का ही अंबार है,
कौन जाने कब लगेगी, किस ठिकाने जिन्दगी।
किसको हम अपना कहें, जब हम किसी के ना रहे,
कब तलक आख़िर चलेगी, इस बहाने जिन्दगी।
खून से सींचा जिसे, वह चमन मुरझाने लगा,
अब भला कैसे कटेगी, रामजानें जिन्दगी।
चार दिन की चाँदनी में, गर न कोई गैर हो,
फिर तो आयेगी यकीनन, सिर झुकाने जिन्दगी।
गर समता की चाहत है तो
इस चार दिवस के जीवन में,
करना घमण्ड बेकार सखे।
उसमें भी सुन्दरता कब तक,
इस सत्य को भी स्वीकार सके।
काया की क्षणिक सुघरता पर,
ना ये जीवन कुर्बान सखे।
क्षणभंगुरता इसकी कहती,
जारी रखना अभिमान सखे।
कल खुशियाँ जिनपे छायी थीं,
दुःख की बदली ने घेरा है।
यह चक्र न थमने वाला है,
ये जग तो रैन बसेरा है।
हंसते देखा रोते देखा,
दुनिया की है रीत यही।
अरि की घात कहीं देखा तो,
अपने भी मनमीत यहीं।
मानव-मानव से जलता है,
ऊँच-नीच की खाईं देखी।
हुए खोखले रिश्ते सारे,
आपस की कटुताई देखी।
गले मिलें होकर संकल्पित,
अब ना कोई बहाना होगा।
गर समता की चाहत है तो,
सबको गले लगाना होगा।
आखिर क्यूँ?
कभी लोग कितना ग़लत सोच लेते हैं?
अपनत्व भरा स्नेह, जल जाता है कूड़े की तरह;
सन्देह करने लगते हैं ख़ुद पर,
समाज के झूठे भय से।
वर्षों का परस्पर प्रेम,
पल में चूर-चूर कर,
अभिशप्त कर देते हैं रिश्ते को;
घृणा के ज़हर से।
आखिर क्यूँ?
मानता हूँ न चाहते हुए भी,
सन्देह दूर कर पाने में असफल;
निराश, बेवश,
घुट-घुट कर पी जाते हैं।
अपनेपन को; कड़वे घूँट की तरह। ।
आखिर क्यूँ?
किस भय से
नर्वस हैं, परवश हैं, विवश हैं:
आखिर क्यूँ?
कहने को तो हम आजाद हैं।
फिर क्यूँ?
ये ऊँच-नीच, भेदभाव, बाप बेटे,
माँ-बेटी, शौहर बीबी या यूं कहे
ईसा इंसा के बीच की खाँई,
नित-बढ़-सी रही है,
आखिर क्यूँ?
आखिर क्यूँ?
रोटी
रोटी के लिए जाने कितने, प्रतिपल जीते हैं, मरते हैं।
रोटी के लिए सहोदर तक, आये दिन लड़ते रहते हैं।
कितनों का उदर बड़ा इतना, भर पाती न इज्जत की रोटी।
रोटी की आड़ में नीयत तक, निशि दिन होती जाती खोटी।
अपने भी मुँह बिचका लेते, दुर्दिन की बदली जब छाती।
रोटी के लिए तन-मन गिरवी, पायल घुंघरू तक बन जाती।
कहीं कुत्ते खेलें रोटी से, नहलाये दूध से जाते हैं।
रोटी के लिए घर तक छोड़ा, जंगल भी दूर भगाते हैं।
रोटी की कीमत क्या जानें, जो खेलें किसी की रोटी से।
रोटी के लिए तोड़ती वो, पत्थर पहाड़ की चोटी से।
हम भले चाँद तक हो आये, ईमान बिका रोटी के लिए।
देखो मेरा भारत महान, इंसान बिका रोटी के लिए।
प्रश्न
गर्दिश की गाज गरीबों पर, क्यूँ दिन में हुआ अँधेरा है?
रोता किसान क्यूँ खेतों में, दुःख की बदली ने घेरा है?
दिन रात एक है किये हुए, मौसम का कुछ परवाह नहीं
पी जाते हैं विष का प्याला, क्यूँ आती मुख से आह नहीं?
क्यूँ बेवश बन जाया करते, क्या बचा नहीं कोई उपाय?
बेदाग बचा है कौन क्षेत्र, मिल रहा कहाँ पर खरा न्याय?
पानी तक मिले न भूखों को, जिन्दा दफनाये जाते हैं
क्यूँ विवश विलखती बहुओं के, अरमां सुलगाये जाते हैं?
चल रही है नफरत की आंधी, अपनेपन को क्या हुआ आज?
निस्वार्थ भाव है कितनों में, क्यूँ मौन हो रहा ये समाज?
फूल
रंग-बिरंगे, प्यारे फूल,
सुन्दर, सुरभित न्यारे फूल।
जाड़ा, गर्मी हो या बरखा,
कभी न हिम्मत हारे फूल।
विविध रंग में एक साथ मिल,
सुन्दर हार बनाते फूल।
हिन्दू-मुस्लिम, सिक्ख-ईसाई,
अलग नहीं समझाते फूल।
काँटों में हो भले बसेरा,
हर पल हंसते-गाते फूल।
दुःख में भी न धीरज खोना,
हमको सदा सिखाते फूल।
सुरभित कर जग चलें नेक पथ,
ऐसी राह दिखाते फूल।
कर्मवीर पग हों जिस पथ पर,
कदम-कदम बिछ जाते फूल।
विन्ध्येश्वरी प्रसाद ‘विन्ध्य’
वाराणसी
यह भी पढ़ें-