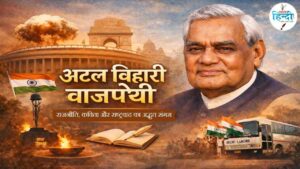कासे कहूँ दुखड़ा
Table of Contents
गणपति बप्पा मोरया – Ganpati Bappa Morya
गणपति बप्पा मोरया – Ganpati Bappa Morya
गणपति, देवगणों में प्रथम पूजनीय। शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती का सृजन। शिव पुत्र। शक्ति और शिव का संतुलन ही बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। सदमार्ग पर प्रेरित बुद्धि ही समस्त मंगलकार्यों का विरोध करती है। इसी विवेक बुद्धि की याचना करते हैं हम मंगल मूर्ति गणपति से। जब विवेक हमारे कार्य का नियामक होता है तभी निर्विध्न लक्ष्य प्राप्ति होती है और इसी अभीष्ट सिद्धि के लिए हम सर्वप्रथम वंदना करते हैं वरद हस्त गणपति की।
गणपति बुद्धि निधान हैं। पुराकाल में देवों में प्रथम पूजनीय कौन? जब यह प्रश्र उठा, तो उन्होंने अपने बुद्धि बल के सहारे यह पदवी सहज ही प्राप्त कर ली। अन्य देवगण जहाँ पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने-अपने वाहन पर आरूढ़ हुए, वहाँ गणपति ने अपने माता-पिता की परिक्रमा मात्र से ही यह कार्य सहज संपन्न कर लिया। सच ही तो है माता-पिता ही तो सम्पूर्ण सृष्टि हैं, उनकी परिक्रमा कर ली तो धरती पर कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता।
उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। उनके पावन मनोहर रूप का दर्शन करने पर यह बात पूर्णत: स्पष्ट हो जाती है। उनका विशाल सिर उनकी व्यापक बुद्धि का परिचायक है। नीर-क्षीर विवेक वाली उनकी बुद्धि का परिचय हमें उस समय मिल जाता है जब महर्षि वेदव्यास अपने विराट महाकाव्य महाभारत की रचना करने वाले थे। महर्षि के मन में बहुत तीव्रता से भाव-उच्छलन हो रहा था, ऐसी स्थिति में उनको लिपिबद्ध कर पाना असम्भव था।
इसके लिए उन्हें एक दक्ष लिपिक की आवश्यकता थी। ऐसे समय में गणपति जी ने उनकी समस्या का निदान किया, और इस जटिल कार्य को सहर्ष करना स्वीकार किया। गणपति की लेखन गति बहुत तीव्र थी, उन्होंने महर्षि के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि उनका लेखन कार्य निर्बाध चलना चाहिए। यदि उनकी लेखनी क्षणांश को भी रूकी तो वे यह कार्य बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। गणपति का प्रस्ताव इतना सरल नहीं था। उद्दामगति से उठते भावों को छंदबद्ध करने और काव्य रूप देने में व्यास जी को कुछ समय तो लगना ही था।
वे दुविधा में पड़ गए, लेकिन शीघ्र ही एक सुंदर समाधान भी सहज रूप में उनके मन में आ गया। उन्होंने गणपति के प्रस्ताव को सशर्त स्वीकार किया। जिसके अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि ऋषि जो भी काव्य रचना करेंगे, गणपति उसका भाव आत्मसात करने के बाद ही उसे लिपिबद्ध करेंगे। गणेश जी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और इस प्रकार विश्व के सबसे बडे़ महाकाव्य की रचना संपन्न हुई। धन्य हैं ऐसे कवि और ऐसे लिपिकार।
गणपति का प्रशस्त भाल, उनकी संकीर्णता रहित बुद्धि की व्यापकता का प्रतीक है। उनकी विशाल गज सूंड उनके अपार शक्ति सामर्थ्य की द्योतक है। वे अपनी इस कर से जहाँ एक ओर वृक्ष के समान बड़े-बड़े अनिष्टों को नष्ट कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर सूचिका (सुई) के समान छोटे से छोटे गुण के भी ग्रहण कर सकते हैं।
उनकी गुणग्राहकता सर्ववंदनीय है। बुद्धिमान सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उनकी शक्ति सदा निर्बलों की सहायक और आक्रांताओं की विनाशक है। गजानन के सूक्ष्म नेत्र त्रिकालदर्शी हैं। उनमें अंतर्मन में झांकने की क्षमता है। जैसे सूर्य की किरणों के समक्ष कोई अँधेरा टिक नहीं पाता, उसी प्रकार हमारे मन के दूषित विकार, उनकी सूक्ष्मभेदिनी अंतर्दृष्टि के समक्ष तिरोहित हो जाते हैं। उनकी स्नेहिल दृष्टि सज्जनों को अभयदान देती है और दुर्जनों को उनके छल-कपट से मुक्त करती है।

गणपति लंबकर्ण हैं। सबकी सुनते है श्रव्य अश्रव्य का विचार कर तदनुसार आचरण करते हैं। सूप के समान साथ-साथ को गृहण कर, थोथा यानी अंसार को त्याग देते हैं। उनका एक दंत अद्वैतवाद को दर्शाता है। वे अहं के जनक द्वैत से परे हैं, क्योंकि यह अहम ही अहंकार का पोषण करता है और संसार के दुःख का कारण बनता है। उसमें विविध प्रकार के वैषम्य लाता है। विवाद और युद्ध में परिणत होता है। आत्मरूप से मिलने में बाधक होता है। अद्वैत का भाव बंधुत्व और एकता का संदेश देता हैं। एकदंत त्याग का संदेश देता है। बिना त्याग के कल्याण संभव नहीं।
गणपति की चार भुजाएँ अपार शक्ति से भरी हैं। उनकी गति चारों दिशाओं में है। उनके हाथों में सुशोभित वस्तुएँ भी विविध भाव प्रकट करती हैं। उनके एक हाथ में कमलपुष्प है। कमल संस्कार, कोमलता, पावनता का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में परशु या कुठार है, जो हमारे समस्त संशयों, कुकर्म और विषय वासनाओं केँ बंधनों को जड़ मूल से काटने में सक्षम है। उनका परशु सभी भौतिक लालसाओं पर कुठाराघात कर हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। बप्पा के एक हाथ में मोदक है, जो हमारे सत्कार्यों का मधुर फल है।
संयमित बुद्धि से किया गया कार्य सदा सुखद होता है। गणपति का चौथा हसरत, अभयदान की मुद्रा में उठा वरद हस्त है। यह सभी को मंगल आशीर्वाद देता है। उनके चरणों में मिष्ठान का एक पात्र है, जो हमारी चंचल और लालची इंद्रियों के, प्रभु चरणों में समर्पित होने का भाव दिखाता है। उनका लंबोदर सर्वग्राही है। समस्त अच्छाइयों और बुराइयों को उदरस्थ कर, निरंतर विकास की ओर बढ़ना ही तो सम्यक प्रगति है।
मूषक गणपति का वाहन है। यह समसत जीवों में सबसे उपर चंचल है। इस पर सवारी करना अर्थात् अपनी बेकाबू इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। यह मात्र गणपति की कृपा से संभव है। उनका एक चरण धरती और एक पद्मासन की मुद्रा में है। विवेकवान धरती पर रहते हुए भी उससे ऊपर होता है। यथार्थ से जुड़ा होकर भी आदर्श की ओर उन्मुख होता है। ‘तेन त्यक्तेन भुंजीथा:’ यानी त्यागपूर्ण भोग ही उसका लक्ष्य है। वह कमलपत्र के समान जीवन सरोवर में विलंबित होता है, लेकिन भोग रूपी जल की एक बूंद भी अपने पर टिकने नहीं देता। त्यागपूर्ण भोग का यही संदेश गणपति की यह मुद्रा हमें देती है।
इस प्रकार गणपति दिव्याभ हैं। उनकी आभा जगत के कम-कम में व्याप्त है। हम भी उनकी इस दीप्ति से आप्लावित हों, इसी भाव को लेकर हम उनकी आराधना करते हैं, उनको नमन करते हैं और करते हैं उनका मंगल आवाहन-गणपति बप्पा मोरया।
फागुन आया
फागुन आया। बधाई। प्रकृति का एक और कालचक्र पूरा हुआ। प्रकृति ने पूरी ईमानदारी दिखाई। पाले और कुहासे की पूरी तरह विदाई हो गई। नभ नील निरभ्र हो गया। बालारुण भी बादलों का झरोखा खोल खिलखिलाया। उसकी किरणों ने धरती पर सतरंगी अल्पना उकेरी। नव किसलय दल पर पड़े तुहिन कण इनका स्पर्श पा रजताभ आभा से दमक उठे। शनै: शनै: सूर्य किरणों का ताप बढ़ने लगा और इस आतप से तपकर शस्य भरे खलिहान सुनहरे हो गए। पीताभ बालियाँ झूमने लगीं।
टेसू, पलाश, कचनार ने धरती पर फूलों का मेला सजा दिया। मंथर, शीतल वतास पुष्पों की सुगंधि क्षटे बहक उठी। पराग धरती पर केसर बन बिखर गया। तरू तृण मस्ती से झूमने लगे। दृष्टि का उत्सव-सा हो गया और हो क्यों न; फागुन आया है। प्रकृति का फगुआना तो बनता ही है। वासंती किशोरी फाल्गुन की दहलीज़ पर क़दम रखते ही नवयौवना हो गई है। हरियाली की चुनरी उसके सिर से सरक-सरक जा रही है।
कलियों का प्रस्फुटन उसकी मनहर स्मित है। खिले पुष्प उसका आनन है। पुष्प पराग उसके मृदुगात का सौरभ है। विहग अपने कलरव से उसके सौंदर्य की विरूदावलि गा रहे हैं। भ्रमरावलि साथ झंकृत कर रही है। प्रकृति ने अपने वैभव का अमूल्य कोष, उदार मना, मुक्तहस्त उस पर लुटा दिया है। इठलाता, मदमाता, अबीर उड़ाता फागुन आ ही गया।

फागुन का आगमन मेरे मन में एक प्रश्र जगा रहा है॥ प्रकृति को अनगिन सौगातें देने वाला यह फागुन क्या कभी मानव मन में भी आएगा? मानव-प्रकृति को भी सरसाएगा। आज मानव का मन पतझर हो गया है। जड़ता, द्वेष, मोह, अहंकार, सर्वार्थ, संशय के घनों ने उसके अंतस-आकाश को अंधेरे से ढक दिया है। आशा, प्रेम, विश्वास की कोई भी उजास उसमें नहीं झिलमिलाती। मन सूखा, कंटीला ठूंठ हो गया है। हरियाली की एक भी चिनगी नहीं है, जिसके सुखद, स्नेहिल ताप का स्पर्श पा उसके जीवन में आशा का अंकुर जाग सके। रोज़-रोज़ नए-नए विवाद, उलझन, समस्याएँ ही पैदा हो रही हैं।
अकेला पन, बेचारगी, संवेदनहीनता ही उसकी नियति बन गई है। बुद्धि का दुरुपयोग कर अपने ही विनाश का साजो-सामान जुटा रहा है। एक की बर्बादी में दूसरे को अपने सुख का मंज़र नज़र आ रहा है। अधिकारों के प्रति आवश्यकता से अधिक जागरूकता, कर्त्तव्यों के प्रति नितांत उदासीनता, देश और समाज के पतन का कारण बन रही है। मानव प्रकृति की यही रूक्षता उसकी सभी उपलब्धियों को व्यंग्य बना रही है। सभ्यता के नाम पर दिनों दिन असमर्थता ही विकास पा रही है।
काश! यह फागुन मानव मन में भी आता, तो उसके मन से भेदभाव और अज्ञता का कुहासा छंट जाता। आशा के सूरज जगमगाते। कल्याण, प्रेम, परोपकार के भाव जनजीवन को मधुर बना देते। हर प्राण में समाई मौन पीड़ा मुखर हो जाती। हर प्रश्र उत्तर पा लेता। देश-राग पूर्ण समर्पण से गुंजित होता। व्यष्टि समष्टि को समर्पित होता। निराशा और वैमनस्य से निस्तार होता।
मैं ऐसे ही फागुन के अभिनंदन को आतुर हूँ। यह फागुन ही सार्थकता देगा तन को, मन को, गगन और धरती को, जन-जन को, कण ।कण को। चेतना के संवाहक बन कर, से मनभावन, फागुन तुम जल्दी से आओ। जड़ता होलिका का दहन करो और रंगों की आभा से दिसि-दिसि अनुरंजि तो कर दो। फागुन तुम्हारा स्वागत है।
ऊधौ मन नाहीं दस-बीस
(कृष्ण-कथा का एक मार्मिक प्रसंग)
कृष्ण-कथा भाव, प्रेम और ज्ञान की अनुपम मंदाकिनी है। इसका हर प्रसंग अद्भुत है, अलौकिक है। भ्रमरगीत भी कृष्णकथा का एक मार्मिक प्रसंग है। कंस के निमंत्रण पर पिता नंद लाल के साथ, कृष्ण-बलराम मथुरा गए हैं। कंस ने उन दोनों को धनुर्यज्ञ देखने का निमंत्रण दिया है, पर सब जानते हैं, यह स्नेह-निमंत्रण नहीं है, यह एक षड़यंत्र है। कंस की कुटिल दृष्टि तो कृष्ण-जन्म से पहले ही उनके विनाश पर है। उन्हें मारकर ही तो वह निशंक हो पाएगा। कृष्ण के मथुरा-गमन से दुखी और डरे हुए हैं ब्रजवासी। गोप-गोपियाँ, नंद-यशोदा, ग्वालबाल, गौ-वत्स और यमुना की लहरें, जिन्हें विष से अमृत बनाया था उनके लाड़ले कान्हा ने। ब्रजवासियों का वश चलता तो कभी न जाने देते, अपने नयनतारों को मृत्यु के मुख में, पर—।
यह पर अपने में छिपाए है सबकी विवशता, दुर्दांत क्रूर शक्ति से भय और अपने प्रिय कान्हा-बलराम से चिर विरह। कृष्ण आश्वासन दे गए हैं, “जल्दी लौट आऊंगा मैया। मेरे लिए माखन निकाल कर रखना। मथुरा में कहाँ मिलेगा ऐसा माखन?” मैया की आंखों में तो जमुनजल से भी ज़्यादा आंसू भरे हैं। गोपियों के उलाहने थम ही नहीं रहे हैं। सब कृष्ण के आश्वासन की सच्चाई जानते हैं। पर क्या कर सकता है कोई? अंततः चले ही गए दोनों अक्रूर के साथ मथुरा।
समय तेजी से भाग रहा है। कंस-वध भी हो गया। माता देवकी और वासुदेव जी को कारागार से मुक्ति भी मिल गई। मथुरा में महाराज उग्रसेन का सुशासन भी स्थापित हो गया। कुब्जा भी रूपवती हो गई। सुदामा भी रंक से राजा बन गए। इतना कुछ हो गया, पर जो न हुआ, वह था ब्रजवासियों की प्रतीक्षा का अंत। न मिला नंद-यशोदा के वात्सल्य को अवलंब और न ही हुआ प्रेमाकुल राधा की विरह-ज्वाला का शमन। सब की प्रतीक्षा, चिरप्रतीक्षा बन चुकी है। उनके लिए समय मानो थम-सा गया है, जैसे वह भी कृष्ण की वापसी के लिए प्रतीक्षा कर रहा हो। कृष्ण तो जैसे ब्रज को बिसरा ही बैठे हैं।
लेकिन इससे कोई निराशा नहीं। पता है कृष्ण अवश्य आएंगे। कहकर जो गए हैं। रोज़ मैया कान्हा के लिए ताज़ा माखन मथती हैं, सबकी नज़र से बचा उसे खूंटे पर ऊंचा लटकाती है। न जाने कब दबे पांव आ जाए, उसका नटखट लल्ला। रूठ जाएगा माखन न मिलने पर। कैसी है, माँ की यह ममता, जो समय के इतने बड़े अंतराल को झुठलाना चाहती है। भूल गई है कि कान्हा अब छोटा बच्चा नहीं है, युवा हो गया है। मधुरा का राज्य-संचालन उसके कुशल हाथों में है। बावरी राधा अपनी नीली चुनरी के पल्लू से, बार-बार कृष्ण की मुरली को पर्याय से पोंछती है। उसके लिए इधर-उधर भटक कर मयूर-पंख एकत्र करती है। कितना खुश हो जाएगा वह यह देखकर और गोपियाँ, रोज़ सुबह-सवेरे दिनभर का काम निबेट, उस रास्ते पर आ खड़ी होती हैं, जिस पर से बरसों पहले कृष्ण उन्हें छोड़कर, दो-चार दिन में लौटने को कह कर मथुरा गए थे। प्रतीक्षा का यह क्रम अनंत है, लेकिन सुखद आस भरा है।
और उधर कृष्ण मथुरा में हैं। राज कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसा नहीं कि वे ब्रजवासियों को भूल गए हैं। ब्रज की, नंद-यशोदा की, ग्वालबालों की, यमुना के कछारों की, गोपियों की, विशालाक्षी राधा की याद रह-रह कर, उनके मन में कसक उठती है। उनका तन मथुरा में हैं, लेकिन मन ब्रज में है। जो आनंद ब्रज में था, वह इस स्वर्णनगरी मथुरा में कहाँ। वृंदावन की कुंजगलियों में, ग्वाल सखाओं के साथ मिलकर की गई नटखट नादानियाँ, वह गो-दोहन का मनोरम दृश्य, उनकी शैतानियों से परेशान, बार-बार ब्रज की गोपियों के उलाहने सुनती और उन्हें बचाती मैया, क्या यह सब भुला देने की बात है। कृष्ण अपने मन की व्यथा अपने परम ज्ञानी मित्र उद्धव को सुनाते हैं-
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं।
हंससुता की सुंदर कगरी, अरू बृच्छन की छांहि।
उद्धव ठहरे काम काजी आदमी। प्यार-व्यार से उनका कोई वास्ता नहीं। कृष्ण का रोज़-रोज़ का खटराग सुन कर झुंझला जाते हैं, “बंद करो यह ब्रजपुराण। छोड़ो भावुकता, ज्ञानी बनो” कृष्ण स्नेह-फटकार सुनकर बस मुस्करा देते हैं। बात आई गई हो जाती है। जैसे तैसे राज-काज में मन लगाते हैं। लेकिन सोने पर सुहागा हैं गोपियाँ। रोज़ संदेशे भेजती हैं, पातियाँ पठाती हैं। ब्रज से मथुरा जाने वाला कोई पथिक ऐसा नहीं जो माखन दही की हांडी, मयूर पंख, बांसुरी और गोपियों का संदेश लेकर कृष्ण के पास न आया हो। इसी बेगार के डर से लोगों ने अपना रास्ता ही बदल लिया है।
गोपियों के हर संदेश में एक ही व्याकुल पुकार है, “कब आओगे, कब आओगे।” संदेश मिलते ही कृष्ण प्रतिपल विकल और विकल, भावुक और भावुक हो उठते हैं और उसी वेग से बढ़ती जाती है उद्धव की खिझलाहट। खीझ कर कहते हैं, “कृष्ण! तुम एक बार ब्रज जाकर इन्हें समझा क्यों नहीं आते?” कृष्ण इस प्रस्ताव पर एक दम हथियार डाल देते हैं, “मित्र, मुझसे यह नहीं होगा, हाँ, तुम ही मेरी ओर से उन्हें समझा आओ। बड़ा उपकार होगा।”
उद्धव कृष्ण के अनुरोध को सहर्ष स्वीकारते हैं। “ठीक है, मैं ही कुछ करूंगा। इन ब्रजवासियों को भावना और मोह के भंवर से बाहर निकालना ही होगा।” कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त निकालकर, एक विशेष प्रयोजन लेकर ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं। कृष्ण यात्रा के लिए उन्हें अपना रथ देते हैं और अपनी ही वेषभूषा में उन्हें ब्रज जाने का परामर्श देते हैं। उद्धव ज्ञानी हैं, पर सरलमना हैं, कृष्ण के आग्रह का कारण नहीं समझ पाते। उनके सुझाव को सहज स्वीकार कर लेते हैं और उनके रथ पर, उनके जैसी ही रूप-सज्जा धारण कर, अपने अभियान के लिए प्रस्थान करते हैं। संयोग की बात है कि उद्धव की देहयष्टि और रंग भी कृष्ण जैसा ही है। अपने इस परिधान में वे कृष्ण जैसे ही लगते हैं। कृष्ण स्नेह पूर्वक मुस्कराते हुए उन्हें विदा करते हैं।
उधर गोपियाँ अपना दिन भर का चूल्हा-चौका निबटा कर, प्रतिदिन की भांति मथुरा से ब्रज आने वाले रास्ते पर, कृष्ण की प्रतीक्षा में खड़ी हो जाती हैं और कृष्ण की अनंत चर्चा शुरू हो जाती है। अचानक ही उन्हें मथुरा की ओर से आता एक रथ दिखाई देता है। उसमें बैठा व्यक्ति दूर से कृष्ण लग रहा है। बस फिर क्या? पूरे ब्रज में शोर मच जाता है। उतावला पन हर बंधन तोड़ देता है। वृंदावन की गली-गली में यह शुभ समाचार उड़ान भरने लगता है:-
कोऊ आवत है तन श्याम।
वैसोई रथ, वैसोई उठिए बैठनि, वैसोई छवि धाम।
देखो-देखो, कोई आ रहा है। वैसा ही सांवला, वैसा ही पहनावा, वैसा ही उठने बैठने का ढंग, वैसा ही सलोना। कृष्ण के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आने दो इस छलिया को। ऐसा मज़ा चखाएंगे कि मैया भी न बचा पाएगी। पूरा नगर कान्हा की अगवानी के लिए इकट्ठा हो जाता है। लेकिन रथ के समीप आते ही उनकी आशा-निराशा में बदल जाती है। कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से खिले मुखकमल मुरझा जाते हैं। निराशा गुस्सा बन कर बहरूपिए उद्धव पर फूट पड़ती है। ” कौन हो रहे तुम छलिया? हमारे कृष्ण का रूप धारण कर क्यों हमें चलने आए हो? बोलो, लाज नहीं आई तुम्हें?
प्रेम का यह आवेश देखकर, उद्धव हतप्रभ हो जाते हैं। उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। किसी तरह अपना परिचय देते हैं। उद्धव कृष्ण के सखा हैं, यह जान कर गोपियाँ खुश हो जाती हैं। वे उनके लिए कृष्ण की संदेश पाती लाए हैं। प्रश्नों की बौछार शुरू हो जाती है उद्धव पर। सब प्रश्र एक ही भाव प्रकटा रहे हैं:-
हमको लिख्यौ है कहा?
हमको लिख्यौ है कहा?
अब क्या बताएँ उद्धव इन प्रेम-बाबरियों को। जो कहने आए थे, वह भी भूल जाते हैं। गोपियों को सांत्वना देते-देते उनका ज्ञान-आवेग दूध के उफान की तरह बैठ जाता है। बुद्धि-क्षमता क्षीण हो जाती है। अपनी ज्ञान, योग, निर्गुण ब्रह्म की बातें उन्हें बेमानी लगने लगती हैं। फिर भी एज अहंकार सिर नहीं झुकाता। वह गोपियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं। कृष्ण को भुला कर निर्गुण ईश्वर की आराधना का उपदेश देते हैं।
गोपियाँ बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनती हैं। फिर विवशता जताती हैं। किसी भी काम को करने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए और उनके पास तो मन ही नहीं है। वह तो कृष्ण चुरा कर अपने साथ ले गए। वह चाह कर भी उद्धव की बात नहीं मान सकतीं। दस बीस मन होते तो तुम्हारी बात सिर-आंखों पर रख लेते। लेकिन विवशता है, क्या करें:-
ऊधो मन नाहिंन दस बीस
एक हुतौ हो गयो स्याम संग, को अवराधै इस।
ऊधो उनके भोले तर्कों के सामने अवाक हैं। गोपियों की प्रेमविह्वलता की पावन-जल धारा उनका सारा ज्ञान बहा कर ले जाती है और वे समझ जाते हैं, मन नाहिंन दस बीस। गोपियों की तो बात ही क्या, अब तो स्वयं उनका मन उनके बस में नहीं है। उनका ज्ञान अहंकार चूर-चूर हो, प्रेमाश्रुओं में बह गया है। मन कर रहा है कि उड़ कर कृष्ण के पास पहुँच जाएँ। उनसे कहें, ” जाओ कृष्ण! ब्रज तुम्हें पुकार रहा है। जाओ, अविलंब जाओ उनके पास। क्योंकि कृष्ण का मन भी तो ब्रज में बसा है। धडकता है ब्रज के कण-कण में। विचरता है ब्रज की कुंज-गलियों में। बार-बार आतुर हो पुकारता है:-
मन नाहिंन दस-बीस।
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै
संसार एक अथाह, अपरिमित सागर। जिसमें इच्छाओं की उत्ताल तरंगें प्रतिपल तरंगायित हैं। अनवरत सफलता-असफलता के किनारों से टकरातीं, जूझतीं, बनतीं-बिगड़तीं हैं। असफलता, निराशा दे रही है। सफलता, अहंकार का पोषण कर रही है। असफलता, कर्म से परे ले जा रही है। सफलता, अपने को कर्ता-धर्ता मान, नियामक होने का भ्रम उपजा रही है। असफलता मन में हीन भाव भर रही है, सफलता, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने, और दूसरों को तुच्छ समझने का अहं जगा रही है।
दोनों ही स्थितियाँ सुख पाने की दिशा में ले जाने में अक्षम हैं, अतः अप्रियऔर अवांछित हैं। तो क्या किया जाएँ, ऐसी स्थिति में? मन तो निरंतर सुख की खोज में जहाज़ के काग-सा व्याकुल है। कैसे मिलेगा सुख? इच्छाओं का बलपूर्वक दमन करने से, या उन्हें उन्मुक्त छोड़ देने से?
वस्तुतः दोनों ही सुख प्राप्ति की राह नहीं हैं। सुख मिलेगा, संयम से, नियंत्रण से, विवेक पूर्ण स्थिरता से। भटकाव मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। साधन का औचित्य और साध्य की श्रेष्ठता ही, सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इस मार्ग पर चलने के लिए प्राणों में विश्वास और कर्म में समर्पण भरना होगा। समर्पण-समष्टि के प्रति, विश्वास-व्यष्टि के प्रति। हमारा कोई भी कार्य समष्टि के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। सर्वहित के श्रेयस पथ पर चलते हुए, हमें न तो असफलता-निराशा में धकेल पाएगी और न ही सफलता हमारे अहं का पोषण कर पाएगी।
कर्मतंत्री के तार जब सहज कसे होंगे, तभी तो मधुर राग झंकृत होगा। मन के भटकाव को स्थायी विराम मिल जाएगा। सुख पाने की चाह में, यहाँ से वहाँ तक उड़ान भरती व्याकुलता शमित होगी, और ईश्वर रूपी जहाज़ का आश्रय ले, वह स्वयं को कृतार्थ समझेगा और उसका कृतज्ञ मन पुकार उठेगा-
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै।
जैसे उड़ि जहाज़ को पंछी, फिर जहाज़ पर आवै।
मैं नहीं माखन खायो
मुख पर माखन लपेटे, दोना पीठ पीछे दुराए, होंठ लटकाए, बिसूरता, पूरी ताकत से अपने को छुड़ाने की कोशिश करता, असमर्थ, विवश, धिसटता नंदलाला। कान्हा की बाँह कसकर पकड़े, उसे नंद भवन की ओर ले जाती, बड़बड़ाती गोपी। कान्हा बीच-बीच में धरती पर बैठ जाता है, पसर-पसर जाता है, लेकिन गोपी भी उसे छोड़ेगी नहीं। कान्हा के गुस्से और हैरानी का कोई ठिकाना नहीं। न जाने क्यों बैरिन बन गईं हैं ये सारी गोपियाँ उसकी? क्या किया है उसने? खुद ही तो बुलाती हैं रोज-रोज। “कान्हा रे! तेरे लिए ताज़ा माखन मथकर रखा है, दही जमाई है। आ जा, ज़रा चखकर तो देख।” और आज जब ग्वाल-बालों से फुर्सत पाकर, गया माखन-दधि चखने, तो यह दूसरा ही बखेड़ा खड़ा कर दिया इस गोपी ने। समझ लूँगा इस सखी को भी। अभी तो मैया की ‘सोंटी’ से बचना है। वैसे मैया है बहुत भोली। बेचारी गैया है बिल्कुल। कह दूूँगा:-
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
और वह झट पतिया जाएगी। तब मज़ा आएगा गोपी की सूरत देखकर और हुआ भी ऐसा ही। मैया ने उलाहना सुनकर डाँटा, कान्हा को नहीं, गोपी को। बोली, “मेरा कान्हा क्या कोई नदीदा है, जो तेरा माखन खाने जाएगा। जरा, झाँक कर तो देख, नंद जू के कोठार में। माखन-दधि की कोई कमी है क्या? हुंह! आ जाती हैं रोज़ रोज। मेरे लल्ला पर झूठा लांछन लगाने।” जसुमति की फटकार सुन कर गोपी का मुँह उतर जाता है। और कान्हा माँ के कंठ में दोनों भुजाएँ डालकर, गोपी की ओर देखता है, जीभ निकाल कर फिराया है, मुस्कराता है। गोपी खीझ कर, बड़बडाती हुई लौट जाती है। माँ लाल पर बलिहारी जाती है, उसकी बलैयाँ लेती है।
आज एक कान्हा और भी है, जो बिसूरता है, “मैं नहीं माखन खायो।” माखन खाना तो बहुत दूर की बात है, माखन होता कैसा है, उसे तो यह भी मालूम नहीं। माँ अपने आँसू पीकर उसे झूठ-मूठ फुसलाती है, “अरे मेरे लल्ला! अभी तेरा बापू आएगा, तेरे लिए दूध-मिठाई लाएगा, अभी तू यह रोटी खा।” और दुबासी-तिबासी रोटी का सूखा टुकड़ा उसके हाथ में पकड़ा देती है, जिसे उसका लाड़ला कान्हा दूर फेंक देता है। मचलता हुआ, पैर पटकता हुआ, ज़मीन पर लोट जाता है। जसुमति खीझ जाती है। उसे चुपाने का निष्फल प्रयास करती है। कान्हा और ज़ोर से बुक्का फाड़कर रोता है।

मचलता हुआ, माँ को लातें मारता है, काटना चाहता है। दो दिन की भूखी मैया गुस्सा जाती है। झल्लाकर उठती है। दोहत्थड़ मारती है कान्हा की नंगी-दुबली पीठ पर, “मर नासपीटे, टिक्कड़ फेंकता है।” कान्हा और ज़ोर से चीख-चीख कर रोता है। मुँह जोरी करता है, “फेंकूँगा, मुझे नहीं खाने ये टिक्कड़। मुझे मिठाई दे, दूध दे।” माँ जसुमति एक हाथ और देती है कसकर, बिलखते कान्हा की पीठ पर “दूध पिएगा, अभागे।” और दूसरे हाथ से अपना कपाल ठोकती, अपने नसीब को कोसती है। कान्हा की रूदन-बाँसुरी का स्वर फटा-फटा जा रहा है।
क्या यशोदा माँ का दिल आज पत्थर हो गया है, या उसकी ममत्व-धार सूख गई है, ऐसी जम गई है, पाषाण हिम खंड सी, कि वह कान्हा के रूदन-ताप से भी नहीं पिघलती। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। ममता दब गई है परिस्थितियों की कठोर शिला से। कलेजा हूकता है उसका, कान्हा का रूदन सुन-सुन कर। पर क्या करे वह? कैसे लाकर दे अपने कलेजे के टुकड़े के माखन-मिश्री। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद भी वह भूखी है और भूखा है उसका लाल। सो गया है बिसूरता-सिसकता। मैले गालों पर आंसुओं की मैली लकीरें हैं। और उसके लल्ला का बापू, लुढ़का पड़ा होगा, किसी पटरी पर, दारू पीकर, औंधा, धुत।
रात गए, होश आने पर घर आएगा। गालियाँ बकता, जसुमति को धकियाएगा, पीटेगा और चित्त पड़ जाएगा। झोंपडी की मनहूस कुरूपता और गहरा जाएगी। भोर होते ही अधसोई यशोदा जागेगी। भूखा-थका पिराता बदन ले, कान्हा को जगाएगी और चल देगी कान्हा के साथ, मजूरी की तलाश में। फटे पल्लू में बँधा रोटी का वही टिक्कड़ कान्हा को देगी और बिना कुछ कहे उसे चबाने लगेगा वह। पेट तो भरना ही है। कान्हा ईंट-गारा ढोएगा, लोगों के सामने हाथ फैलाएगा और मैया दूसरों के जूठे बर्तन धोएगी, पोंछा लगाएगी। कब तक होगा ऐसा?
आज पूरा संसार इस स्थिति में सुधार लाने में लगा है। बडे-बड़े व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने, देशों ने जिम्मेदारी ली है। बचपन को उसकी मुस्कान लौटाने का दावा किया है। आकर्षक नारे लगाएँ हैं। पोस्टर छपवाएँ हैं, वोट कमाएँ हैं, लेकिन बचपन आज भी भूखा है। बिलख रहा है, “मैं नहिं माखन खायो।”
आज बचपन का शोषण मात्र आर्थिक अभाव के कारण शारीरिक स्तर पर ही नहीं, मानसिक स्तर पर भी हो रहा है। द्वापर की जसुमति का कान्हा हठ पकड़े बैठा है:-
आजु हौं धेनु चरावन जैहौं।
प्रात होत बल के संग जहिहौं, तेरे कहे न रह्यौ।
जसुमति कान्हा को तड़के ही जगाने का आश्वासन देती हैं, पर जगाती नहीं। यह भी भला कैसा हठ? कच्ची-मीठी नींद से क्यों जगाए माँ कन्हैया को। न जाने कौनसा सपना देख रहा होगा। नन्हा-सा ही तो है उसका लाल। गाएँ चराएगा। कहीं दब-दबा जाए तो? चोट-फेंट लग जाए तो? ग्वालों के साथ गायों के पीछे-पीछे भागकर थक जाएगा। कमल-सा मुँह कुम्हला जाएगा। नहीं, वह तो बिल्कुल नहीं जगाएगी उसे। ज़रा देर रूठेगा, मुँह फुलाएगा, फुला ले। थोड़ी देर में ख़ुद ही आएगा ठुनुकता हुआ, माखन खाने।
और एक आज का कान्हा है। कटवां गिनती गिनता-गिनता, नर्सरी राईम्स गाता, देर रात गए तक सोता है। जसुमति सुबह पाँच बजे का अलार्म लगाती है। कान्हा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच पैक करती है और छह बजे उसे उठाती है, “उठो चुनमुन! नहीं तो लेट हो जाओगे। स्कूल बस छूट जाएगी।” “” ऊँह—, मम्मी, प्लीज, दो मिनट और सोने दो। अभी उठ जाऊँगा। “और करवट बदल कर सो जाता है। माँ तवे पर रोटी पलटने के लिए रसोई में भागती है। ठीक पाँच मिनट बाद माँ की तेज खीझी हुई आवाज़ आती है,” चुनमुन, अरे उठा कि नहीं? “और दो सैकेंड बाद ही जसुमति आ जाती है।
गुस्साती हुई, खिझलाती हुई, चीखती है,” चुनमुन, अरे अब उठता है या दूँ दो? “—-और उसे ज़ोर से झिंझोड़ कर, हाथ पकड़कर उठाती है, पलंग पर बैठा देती है। अलसाया, उनींदा कान्हा पलंग पर बैठा है। उसे तैयार होना ही पड़ेगा। अच्छे बच्चे स्कूल बस मिस नहीं करते। क्या मुसीबत है। नहीं बनना उसे गुड बॉय। आधे घंटे बाद ही, नन्हा चुनमुन अपनी पीठ पर भारी बस्ता लटकाए, स्कूल यूनीफॉर्म में सजा-धजा घर से बाहर होता है। उसकी सज-धज कितनी आकर्षक है। कितना स्मार्ट लग रहा है वह। माँ टाटा-बॉय-बॉय करती है। बस वाली आंटी चुनमुन को बस में घसीट लेती है।
चुनमुन का मन रो रहा है, कौन देखता है यह? दो बजे तक की क़ैद में जा रहा है बेचारा कान्हा। स्कूल से आते ही माँ पूछेगी, “क्या हुआ आज स्कूल में? होमवर्क तो ठीक से नोट किया है डायरी में? आज फिर पानी की बोतल भूल आया?” चलो, यूनीफॉर्म बदलो। हाथ-मुँह धोकर खाने की मेज पर पहुँचो। बस्ता-जूता जगह पर रखो। ” चुनमुन बस्ता पटक कर, जूते को किक मारने की फ़िराक में है।
जब वह खाने की मेज पर होता है, माँ बस्ता टटोलने लगती है। कॉपियाँ खोलकर देखती है। “यह क्या, इतना गंदा काम। आज फिर सात का पहाड़ा ग़लत कर दिया। डिक्टेशन में इतनी गलतियाँ? क्यों?” माँ डाँट कर पूछती हैं। चुनमुन नहीं सुनता। गस्सा हाथ में लिए कार्टून देखता रहता है। माँ झल्लाकर टीवी बंद कर देती है”इस टीवी ने ही सत्यानाश किया है तेरा। चल उठ अब। आधा धंटा हो गया बैठे-बैठे।” कान्हा मन मारकर उठता है। उसका तो जीना ही दूभर हो गया है, पता नहीं वह कब बड़ा होगा? लेकिन उसकी परेशानी से किसी को कोई मतलब नहीं।
चुनमुन को पढ़नी ही होगी यह पढ़ाई, जिसने उससे उसके खिलौने और खेल का मैदान छीन लिया है। उसकी कल्पना को मार दिया है। उसके नन्हे से दिमाग़ में ढेर सारा ज्ञान रटा-रटा कर ठूंस दिया है। क्या यह अन्याय नहीं, शोषण नहीं? चुनमुन खेलना चाहता है, कोई उसे खेलने नहीं देता। क्या ऐसा बचपन, मुरझाया बचपन बनेगा देश का यौवन, उसका भविष्य? बचपन का कुपोषित तन और अविकसित मन करेगा नेतृत्व देश का?
नहीं। सही उत्थान चाहिए तो सुपोषित होने दो बचपन को। दौड़ने दो उसे मैदानों में, उड़ान भरने दो उसकी कल्पना को, बनाने दो उसे उसकी ज़िन्दगी का चित्र खुद। सनने दो गोरज में, तभी तो कान्हा संहार कर पाएगा कंस का। दे पाएगा उपदेश गीता का, मंत्रमुग्ध कर पाएगा अपनी मोहिनी मुरली की तान से अग-जग को। कर पाएगा अपना बचाव यह कह कर:-
“मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो”
जेहि चितवत इक बार
चितवन—आँखों की भाषा। ऐसी भाषा, जो निशब्द होते हुए भी शब्दों से अधिक अभिव्यक्ति-क्षम है। सृष्टि के प्रारंभ से ही चितवन अपनी शक्ति का परिचय देती आई है। आज तो खै़र स्वच्छंद प्रेम और उन्मुक्त सौंदर्य का युग है, लेकिन उस युग में भी जब प्रेम पर बंधन था, तब भी चितवन की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। कालिदास की मृगनयनी शकुंतला हो, या तुलसी की मर्यादा आबद्ध सीता, हो, या सूरदास की विशालनयनी राधा, सभी की चितवन उनके प्रिय को रिझा लेने को पर्याप्त थी। कबीर की विरहिन ने तोअपने आराध्य को ही अपनी चितवन से रिझा लिया था:-
नैननि की करि कोठरी,
पुतरी पलंग बिछाय।
पलकनि की चिक डारि कै,
पिय को लिया रिझाय।
चितवन का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया रीतिकालीन कवियों ने। उनके नायक-नायिका तो भरे ‘भौन’ में ‘चितौन’ के माध्यम से ही बतकही कर लेते थे:-
कहत नटत रीझत खिझत,
मिलत खिलत लजियात।
भरे भौन में करत हैं,
नैननि ही सौं बात।
नयनों की यह भाषा इतनी प्रभावी थी कि छोटे-मोटे छैलाओं की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े सूरमाओं के छक्के छूट जाते थे:-
कहा लडैते दृग किए,
परै लाल बेहाल।
कहुँ मुरली, कहुँ पीतपट,
कहुँ मुकुट बनमाल।
कविवर रहीम ने भी चितवन की महिमा को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया और उस पर अपनी मोहर लगाई:-
जो रहीम जग मारियो,
नैन बान की चोट।
भगत भगत कोई बच गए
चरण-कमल की ओट।
लाख बचने की चेष्टा करो, बच नहीं पाओगे। वैसे नयनबान की यह चोट है बहुत मधुर, जो बिना टिकट त्रिलोक की परिक्रमा करवा देती है। अनेक सजीले संसार दृष्टि के समक्ष उपस्थित कर देती है। मारकर जिलाती है, तो जिलाकर मारती है। मन में मीठी-सी टीस जगा देने वाली यह चोट प्रेमी-युगलों के लिए सदा काम्य रही है:-
अमिय हलाहल मद भरे,
श्वेत श्याम रतनार।
जियत मरत, झुकि-झुकि परत,
जेहि चितवत इक बार।
एक ज़माना था जब चितवन झूठ नहीं बोलती थी। मुखकही की अपेक्षा आँखों की भाषा अधिक विश्वसनीय मानी जाती थी। विद्वान इसी पर भरोसा रखने की सलाह देते थे:-
झूठे जानि न संग्रह,
मन मुँह निकसै बैन।
याहि ते मानौ किए,
बातन को विधि नैन।
लेकिन अब ऐसा नहीं। अब तो नेत्रों ने भी झूठ का अभिनय करना सीख लिया है। मुँह बड़े-बड़े वायदे कर रहा है। प्रेम में जीने-मरने की कसमें खाई जा रही है। बेचारे चाँद-तारों का अस्तित्व दाँव पर लगा है कि न जाने कब कोई सिरफिरा मजनू उन्हें तोड़कर अपनी प्रियतमा के केशों में सजा दे, और नेत्र भी इसकी जोर-शोर से पुष्टि कर रहे हैं। कितना सही झूठ बोलना सीख गई है चितवन। और क्यों न हो ऐसा? ज़माना ही अवमूल्यन का है। ज़माने के साथ चलना ज़रूरी है फिर चितवन का परहेज बेमानी है।
आज अनन्यता का पूर्ण अभाव है। निष्ठाएँ बार-बार टूटती हैं। क्यों? क्या हमारी सौंदर्य निरीक्षक वृति इतनी सूक्ष्म हो गई है कि अतृप्ति ही उसकी आदत बन गई है।
ज्यों ज्यों निहारिए नेैरे ह्वै नैननि,
त्यों-त्यों खरी निकरैसी निकाई।
वाली स्थिति तो अब कदापि नहीं।
अगर ऐसा होता तो होती एकनिष्ठता। होती अनन्यता।
चितवन तब वंचना न करती, बल्कि धन्य हो जाती।
किसी अन्य को निहारने की इच्छा ही नहीं रहती। होती प्रेम की आदर्श स्थिति:-
लोचन मग रामहि उर आनी,
दिए पलक कपाट सयानी।
आज तो नेत्र भटक रहे हैं, चितवन में चंचलता तो है लेकिन मन की निर्मलता नहीं। छिछोरापन आ गया है आज चितवन में। वह सौंदर्य की नहीं, कुरूपता की उपासिका हो गई है। हर ओर वासना, नग्नता और अश्लीलता की तलाश हो रही है। नज़रिया बदल गया है नज़र अपनी ही नज़र से गिर गई है। कुत्सित वासनाओं की पूर्ति होते ही चितवन भ्रकुटि तान लेती है। विचित्र-सा अजनबीपन उभर आता है चितवन में। पल भर पहले के आतुर और लालायित नेत्र नई खोज में लग जाते हैं। चितवन का यह भाव परिवर्तन नैतिक मूल्यों के ह्रास से जुड़ा है। सांत्वना, स्नेह दुलार, आत्मीयता बरसाने वाली चितवन आज विरल हो गई है। प्रतिकार, हिंसा, रोष, तिरस्कार, स्वार्थ भरी आँखें हर जगह दिखाई देती हैं।
नेत्रों की इस भाषा को बदलना ही होगा। निराशा को आशा, पीड़ा को हर्ष में बदलना होगा। भौतिक चकाचौंध से चौंधियाए नेत्रों को पारखी दृष्टि देनी होगी। लाना होगा उन्हें शीतल, कोमल, प्रकाश से आवेष्टित धरातल पर। जहाँ भटकाव न हो। हो केवल संतुष्टि, पूर्णता और समर्पण। चितवन के मार्गदर्शन का यह गुरूभार साहित्यकार के कंधों पर है। साहित्य अपने दायित्व से विमुख नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है।
कछुक दिवस जननी धरि धीरा
बात है त्रेता की। लंका की अशोक वाटिका में “निज पद नयनु दिए, मन राम पदकमल लीन” की स्थिति में बैठीं माता जानकी और सुत पवनपुत्र हनुमानजी। भावाकुल अंतर लिए माँ सीता जी को धैर्य बँधा रहे हैं:-
कछुक दिवस जननी धरि धीरा,
कपिन्ह सहित अइहहिं रधुबीरा,
निसिचर मार तोहि ले जइहहिं
तिहूँ पुर नारदादि जस गैहहिं
“कुछ दिन और धैर्य धारण करो माँ। प्रभु राम आएँगे, राक्षसों का वध कर आपको यहाँ से लेजाएंगे।” कितने सामर्थ्यानुकूल, दृढ़निश्चय भरे, मर्यादित वचन हैं, सुत के माता के प्रति।
कछुक दिवस जननी धरि धीरा
कोई व्यर्थ बात नहीं। जननी को प्रसन्न करने के लिए कोई ‘ठकुरसुहाती’ नहीं। कोई झूठी आस नहीं, कोई झूठी आस नहीं कि अभी ले जाएंगे, इसी क्षण ले जाएंगे। हाँ, ले अवश्य जाएँंगे। यह सौ प्रतिशत निश्चित बात। कुछ दिन तो लगेंगे ही। शत्रु प्रबल है। आक्रमण की योजना बनेगी। कार्यान्वयन होगा, तभी तो होगी जननी की मुक्ति। और सीता भी आश्वस्त हैं आश्वासन पाकर।
‘सीता मन भरोस तब भयहु’
लेकिन आज जननी आश्वस्त क्यों नहीं हो पा रही अपने करोड़ों सुतों के होते हुए भी। नैराश्य तिमिर इतना सघन है कि उजास की कोई भी किरण नहीं फूटती। क्यों लग रहा है उसे कि उसके समर्थ पुत्र उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान की रक्षा में असमर्थ हैं। क्यों न हो निराशा? आज निराशा का स्तर भी दोहरा है। दूर तक जहाँ भी जननी की नज़र जाती है, अँधेरा ही अँधेरा है। घर-प्रांगण में बैठी वृद्धा जननी। उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनी। छाती का दूध पिला-पिला, तन-मन गला दिन-रात एक कर जिन संतानों को पाला, आज वह उन्हीं की आँखों में खटक रही है। संतान विवशता वश बूढ़े माता-पिता को ढो रही है। आत्मीयता भरे निःस्वार्थ सम्बंधों की इतनीकुरूपता अविश्वसनीय लगती है। कैसे बँधाएंगे ये कुरूप सम्बंध माँ को धीर? उर में कसक धारे जननी अधीर बैठी है।
नैराश्य का दूसरा स्तर राष्ट्रव्यापी है। भारत माता उदासीन, मलिन-मना है। तिस पर विडंबना यह कि यहाँ धीर देने वाले पुत्रों की कोई कमी नहीं। खोखले, संवेदनरहित आश्वासनों की भीड़ एकत्र है उसके चारों ओर। सुंदर, आकर्षक शब्द जाल। ” तेरे लिए जिएंगे-मरेंगे का भाव प्रकटाते आश्वासन हर नगर, प्रांत, राज्य, संप्रदाय, जाति, धर्म से अहर्निश मिल रहे हैं। भाषाएँ विविध हैं, शैलियाँ अलग हैं। एक दूसरे से बाजी मार ले जाने की होड़-सी लगी है, लेकिन भारत-जननी रंचमात्र भी आश्वस्त नहीं हो पा रही। हो भी कैसे? राक्षसो को मारकर ही तो उसकी रक्षा करेंगे उसके पुत्र। लेकिन पुत्र तो स्वयं ही असुर हो रहे हैं। कैसा भयानक होता है अपनों द्वारा दिया गया त्रास।
“जाके फटी न पैर बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।”
उसका हर पुत्र स्वयं को उसके सामने आदर्श सिद्ध करना चाहता है। बिना सिर कटाए ही शहीद बनना चाहता है। जननी को भुलाकर सब, हर्ष, सुविधा, उल्लास केवल अपने लिए ही समेट लेना चाहता है। कैसे धीरज दे पाएँगे ये सुत जनना को? ” कछुक दिनों की पीर’ अब दशकों की प्रतीक्षा बन गई है। क्यों न रोए माँ? भारत माता, जो कितनी सदियों बाद तो स्मित-आनना हुई थी, जब उसके पवनपुत्र जैसे पुत्रों ने, रक्तदीप जलाकर परतंन्त्रता के अँधेरे को स्वातन्त्र्य विहान में बदला था॥
मगर अब तो पिछले छह दशकों से देखती आ रही है जननी, कि पूत कपूत बन कर उसका ही ह्रदय विदीर्ण करने पर तुले हुए हैं। भाषा, धर्म, अर्थ, जाति, समुदाय, दलित, शोषित सभी उनके आयुध हैं, जिनका प्रहार वे निरंतर माँ के वक्ष पर कर रहे हैं। जननी के शुभ चिंतको का सारा बुद्धिकौशल आयुध निर्माण में ही तो लग रहा है। और माँ तब भी असुरक्षित है। स्वार्थ, लिप्सा, हिंसा का तांडव करने वाले, उसके ये पुत्र ही में उसके रूदन का कारण हैं।
माँ का धानी आँचल अब मटमैला हो गया है। दिनों दिन धूप-ताप से बदरंग हो रहा है। माँ की चिंता भविष्य में आने वाले बहुत बड़े विनाश के कारण तो नहीं? प्रदूषण की व्यापकता उसका कलेजा सिहरा रही है, थर्रा रही है। नदियों का अमृत जल विष बन रहा है। मलयानिल-सुरभित उसका पर्यावरण अब श्वास लेने योग्य नहीं रहा। पर्वत नंगे-बूचे हो रहे हैं। जंगल दिनोंदिन सिमटते जा रहे हैं। हर कोई दोहन में लगा है, पोषण की किसी को चिंता नहीं। कैसे न रोए माँ?
अन्नपूर्णा कहलाने वाली माँ की आधी से अधिक संतानें भूखीं-प्यासी बिलख रही हैं। माँ ने तो अपना कोष लुटाने में कोई कृपणता नहीं की। वह तो आज भी वसुन्धरा है। वस्तुतः आज उसके पुत्र एक-दूसरे से बाँटने में नहीं, छीनने में लगे हैं। एक के शोषण पर दूसरा अपने वैभव की मीनारें चिन रहा है।
शैशव असमय ही प्रौढ़ हो रहा है। यौवन की उमंग तरंगायित नहीं होती, निराशा का पर्याय हो गई है। कैसे धीर धरे माँ? उसकी बेटियाँ अब भी अनेक प्रकार से प्रताड़ित की जा रही हैं। अनेक आँखें अक्षर ज्ञान से अनजान हैं। सपने अश्रुओं में बहे जा रहे हैं हैं। माँ की धीर अब अधीर हो गई है। उसका रूदन फूट निकला है और उसके समर्थ पुत्रों को उसका विलाप सुनाई नहीं देता। उसका अश्रुपात अनदेखा हो रहा है। अपने ही उजालों में खोए उसके ये समर्थ पुत्र, दीपक तले के अँधेरे को जानते हुए भी, उसे दूर करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। “कछुक दिवस जननी धरि धीरा” में कुछ ईमानदारी होती, तो माँ कोआस बँधी रहती। मुक्ति की आस, सर्वांगीण उन्नति की आस। लेकिन अब तो इसी कारा में रहना होगा, हताश। कब तक? यह एक अनुत्तरित प्रश्न।
लेकिन नहीं, आस तो धरनी होगी। आशा पर आकाश टिका है। उसके सभी पुत्र तो पुरुषार्थ रहित नहीं हैं। कुछ तो हैं ही, जिनके मन-प्राणों में माटी की सौंधी महक महकती है। जिनकी जड़ें धरती में गहरी जमी हैं। जिनकी आँखें अंतरिक्ष पर हैं। जिनकी गति मारुति नंदन की गति है। माँ की व्याकुल पुकार पर अर्पित होने वाले पुत्र आज भी हैं। जो माँ का ऋण चुकाना जानते हैं। जो कह रहे हैं निष्ठा से, ” धीर धर माँ, कुछ दिन और क्षमा कर अपने अज्ञानी पुत्रों को, शायद ये तेरे भूले-भटके पुत्र शाम ढले, तेरी ममता की ओट में आसरा पाने, घर लौट आएँ। अबोध शिशु भी जब अँधेरे में माँ का स्पर्श पहचान लेता है, तो क्या ये उससे भी नादान हैं?
नहीं, इन्हें लौटना ही होगा। अपनी सुखद क्रोड़ में सुला, उजाले की लोरी, तू ही तो इन्हें सुनाएगी। इसलिए धीर धर माँ, कुछ दिन और। प्राची पर लालिमा छिटकने ही वाली है।
जन्म हमार सुफल भा आजु
जन्म हमार सुफल भा आजु। संतुष्टि का भाव और कृतज्ञता ज्ञापन। कृतज्ञता उस परमपिता के प्रति, जिसने हमें दुर्लभ मानव देह प्रदान की और दी वह सद् बुद्धि जिसने हमें इसका सदुपयोग करने की प्रेरणा दी। कृतज्ञता-ज्ञाप्ति के ये क्षण अनिर्वचनीय आनंद से भरे हैं। जीवन में प्रतिपल जिस हरि कृपा का अनुभव किया है, जिसे आँखों से देखा है, उसका वर्णन हो भी कैसे सकता है। ‘गिरा अनयन नयनु बिन बानी’ के भाव भरे क्षण। भावों का सहज उच्छलन शब्दों को असमर्थ बना देता है।
क्यों ओत-प्रोत है मन इस संतुष्टि से? , क्या पा लिया है ऐसा कि प्रसन्नता निस्सीम हो रही है। कूल कगार तोड़ कर बह निकली है भाव-मंदाकिनी। अपार धनराशि, अपरिमित कीर्ति, अजेय शक्ति, सर्वोच्च सत्ता? इनमें से क्या मिल गया है तुम्हें, जो तुम्हें अपना जीवन सफल, सार्थक लगने लगा है? क्या कहा? कुछ भी नहीं। तो किस बात का संतुष्टि गर्व?
बताना ही होगा। गर्व इस बात का कि हम मानवता से जुड़े हैं। भौतिकता से जुड़ाव हमें इससे कोसों दूर पटक देता है। मानवीयता से परे होने का मतलब है अभाव, असंतुष्टि। असंतुष्टि स्वयं से, सबसे, यहाँ तक कि उस प्रभु से जिसने हमें मानव देह दी। धन, शक्ति, यश सभी हममें अहंकार का बीजारोपण करते हैं। इन बीजों से अंकुरित अंकुर देखने में कितने ही आकर्षक और ललक भरे क्यों न हों, हमारे भौतिक अस्तित्व के लिए कितने ही अनिवार्य क्यों न लगें, लेकिन इनका विकास वट वृक्ष के रूप में नहीं, आक के पेड़ के रूप में होगा। छायाहीन, फलहीन। व्यर्थ है वह तरू जिसकी शाखाओं पर पखेरूओं के अनगिन बसेरे न हों, जिसकी पत्तियों से हवा गुनगुनाती हुई नहीं गुजरती,
जिसकी छाया में थका हारा पथिक पलभर विश्राम न पा सके
बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर।
पंथी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर।
व्यर्थ है वह मानव जीवन, जो किसी का आश्रय नहीं बनता। किसी की पीड़ा को दूर नहीं करता। जिसके सुख-दुःख की परिभाषा अपने तक ही सीमित हो। मिथ्या गौरव और अहंकार से भरा व्यक्तित्व, विश्व का सबसे बौना व्यक्तित्व होता है। विनम्रता ही महानता की जननी है। यही विनम्रता ध्वनित होती है इन पंक्तियों में:-
जन्म हमार सुफल भा आजु
प्रभु की किरपा भए सब काजू।
अपने समस्त कार्यों को, समस्त परिश्रम को, समस्त प्राप्तियों को प्रभु-अर्पण कर देना ही जीवन की सार्थकता है। यह कार्य मैंने किया है तभी मुझे अभीष्ट प्राप्ति हुई है; यह भावना मन में क्षुद्रता लाती है। अहंकार को पोषित करती है। दृष्टि को संकीर्ण बनाती है। परिश्रम का फल आशानुकूल न होने पर मन में हीनता का भाव उत्पन्न करती है
जो हमारी गति में अवरोध लाता है। अतः अपने समस्त कर्म और श्रमफल को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है।
करि गोपाल की सब होई
जो अपुनौ पुरुषारथ मानत
अति झूठौ है सोई
इसी विचार धारा का अनुसरण कर, जीवन संघर्ष में लगे रहना ही श्रेष्ठ है। तभी हमें संतुष्टि का सच्चा स्वाद मिलेगा। यहाँ संतुष्टि का अर्थ विराम नहीं है और न ही पूर्णता का भ्रम है। जीवन विराम हो ही नहीं सकता क्योंकि वह सतत प्रवहमान जलधार है। गति ही इसे अमरत्व देती है, उपयोगी बनाती है। अपनी महत्त्वाकांक्षा को विराम मत दो। उन्हें गगन-सा निस्सीम विस्तार दो। उन्हें साकार पूर्ण निष्ठा, लगन और सामर्थ्य से उन्हें साकार करने का प्रयास करो। ये आकांक्षाएँ पूरी होनी ही चाहिएँ क्योंकि ये स्वार्थप्रेरित नहीं है।
ये सत्य, शिव और सौंदर्य की भावना से समन्वित हैं। सर्वमंगल भाव और समर्पित कार्य निष्ठा ही तुम्हें ईश्वर का कृपा पात्र बनाएगी। तुम्हारे मन को सद्-विचारों से युक्त करेगी। तुम्हें उत्साह देगी। तुम्हारे लिए सफलता का हर द्वार खोलेगी। त्याग भाव से किया हर कार्य तुम्हारे मानव जीवन को सार्थकता देगा। नश्वरता अनश्वरता में परिणत होगीऔर सतुष्ट मन बार-बार पुकार उठेगा—
जन्म हमार सुफल भा आजू
वीणा गुप्त
नई दिल्ली
यह भी पढ़ें-