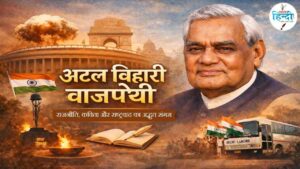कच्चे घर में मां का आंचल
कच्चे घर में मां का आंचल : याद आ रहा है बचपन वाला गांव! जहां पूरे गांव में एक भी पक्का मकान नहीं हुआ करता था। गांव में एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय कंक्रीट से बना, हुआ करता था; वह भी गांव से बाहर! उन कच्चे मकानों से मकानों की दूरी बहुत कम हुआ करती थी। खपरैल मकानों में भी दो मंजिलें भी हुआ करती थीं और उनकी सुंदरता अनुपम हुआ करती थी।
वास्तव में प्राकृतिक वातावरण में हम उन कच्चे मकानों में वातानुकूलन महसूस करते थे। कच्चे मकान एक दूसरे से मिले हुआ करते थे और कोई समस्या होती तो औरतें अंदर से अपने पड़ोसी महिलाओं से बातचीत करके निराकरण, एक दूसरे की मदद भी कर देती थीं।
पंक्तिबद्ध मकानों में जाने के लिए बीच से जो रास्ता जाता था उसे गांव के लोग खोर कहते थे; वह संकरी हुआ करती थी। इस तरह से बगल वाले मकान में रहने वाले पड़ोसी भी दूर नहीं पास ही होते थे। यह एकता और भाईचारा की मिसाल हुआ करती थी। गांव में अपनी – अपनी बर्चस्व की लड़ाई होती थी और बोलचाल भी बंद हो जाता था। लेकिन अगर इज्जत किसी की दांव पर होती तो, दुश्मन भी उसे बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे।
सबसे बड़ी बात उन कच्चे घरों में मां होती थी। खेलते – खेलते दोस्त के घर में ही खाना खाते तो कभी यह महसूस ही नहीं कर पाते थे कि, अपनी मां खाना नहीं खिला रही है और यह मेरी मां का आंचल नहीं है; जो खाना खाते वक्त हवा करते हुए डुल रहा है।
बचपन ऊंच – नीच, जाति – पांति से अनजान, प्रेम जानता है और प्रेम ही बचपन की जाति होती है, धर्म होता है और धन होता है। फिर उन कच्चे मकानों में प्रेम बरसता था और प्रेम बोलता था। गांव में सभी अनाज पैदा होते थे और देशी खाद से उगाया गया मोटा अनाज खाकर सभी निरोगी जीवन जीते थे। और उन कच्चे मकानों में मां का आंचल सुख बरसाता था।
संपत और कौशल जैसे साथी थे जो साथ नहाते और साथ खाते, साथ ही पढ़ने जाते थे। वह दूसरी जाति से थे। अगर हमारे यहां सो जाते और उनकी मां पता करने आती थी तो मेरी मां कह देती, “सो गए हैं, सोने दीजिए सुबह यहीं से पढ़ने चले जाएंगे!”
उनकी अम्मा कहती, “अरे वो तो, अपना के बिस्तर पर सूते हैं, धोना पड़ेगा, मैं सुबह धो दूंगी दीदी!”
तब मेरी अम्मा डांटती उन्हें, “छूत तो, तुम में और हममें है, वह तो बच्चे हैं, मैं तो अपने बेटवा के साथ उन्हें खाना खिलाया करती हूं और उनकी थाली भी धो देती हूं!”
तब संपत की अम्मा कहती, “हमें नरक न भेजें महराजिन!”

तब मेरी मां हंस पड़ती थी और कहती थी कि, “जब तुम मेरे बेटवा को खिलाया करती हो तब, क्या करती हो? पढ़ लिख लें और इनकी शादी कर देंगे, फिर रसोई में नहीं घुसने दूंगी और तुम्हारे घर में यह खुद नहीं खाएगा!”
बरसात में खपरैल से टपकता पानी और मां के आंचल में हम सुरक्षित रहते थे। पिता जी रात भर हमारी सुरक्षा के लिए जागकर बिता देते थे। बहन की कमी नहीं थी। जलेब्बू की बहन मुझे भाई मानती थी और मैं उसे बहन! वह रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी और मां उसे कुछ देती नहीं थी सिर्फ उसे गले से लगाकर चूम लिया करती थी।
मां मथानी में भांकर दूध से घी निकालती थी और मां को हम दूसरी तरफ, दूसरे काम में भेजकर गप्प से माखन मार देते थे। मां आती और कहती, “नुकसान करी इतना खाओगे जो माखन!”
फिर हम कहां मानने वाले थे। मां कंडा बीनने जाती थी और लकड़ियां भी लाती थी। मां के हाथ से पोई रोटी वर्षों हो गए खाए और अब के खाना में वैसा स्वाद कहां होता है! गांव के कच्चे मकानों में एक मकान मवेशियों के लिए अलग हुआ करता था। हम सभी दोस्त लुका – छिपी खेल खेलते थे और खूब धमाचौकड़ी मचाया करते थे। उस मवेशियों के बाड़े में छुपकर कूकी मारते थे और छू जाने पर ढूंढ़ने का काम जो पकड़ जाता, छू जाता वही करता था।
बगीचों में पेड़ों पर लसगड़िया खेल, खेला करते थे और मां को नजर में रखते थे। मां भी खेतों में काम करते भी और लकड़ियां इकट्ठी करते हुए भी, हम सभी दोस्तों पर नजर रखती थी। कच्चे मकानों की अटरिया में हम चढ़ जाते थे। निश्छल मन हमें कोई नहीं रोकता था।
आज गांव के कच्चे मकान नहीं के बराबर रह गए हैं। पक्के मकान में पक्के दिल के लोग रहते हैं। बचपन कोई लुका छिपी नहीं खेलता है और बचपन मोबाइल गेम में खो गया है। बचपन, किशोरावस्था का पता ही नहीं चलता है और जवानी आकर तुरंत बुढ़ापे में तबदील हो जाती है। मोबाइल के तिलिस्म में बचपन अब बचपन नहीं रहा। बाल लीला के सपने अबके माम – डैड, गांव के मम्मी – पप्पा नहीं संजोते हैं।
अब का मनुष्य, मानव जीवन को तरसता है। जवानी छूमंतर होकर, हाय हाय, भागम भाग में पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। तबके कच्चे घरों में, मां का आंचल भलाई फट जाने से पैबंद लगा होता था लेकिन उस आंचल में पलने, बढ़ने और छाया में जो सुख था वह, आज की पक्की वातानुकूलित हवेली में और तमाम विदेशी साड़ी वाले आंचलों में नहीं है।
गांव में नदी सूख गई और कच्चे घर पक्के हो गये। पीपल छांव नहीं है। अंवराई नहीं बची है। मां का आंचल संकीर्ण हो गया है और प्रेम – भाईचारा डूब गए हैं। अब दुलहादीन अहीर की गाय दूध नहीं दे रही है। अब दीपावली में अहीरों की कूक नहीं सुनाई दे रही है। जातिवाद, संप्रदायवाद और धर्मवाद में सबकुछ बिखर गया है।
अब कच्चे घर में मां का आंचल जो बचपन को बचपन बनाया करता था और बचपन में कृष्ण – कन्हैया की तुलना होती थी। जब कच्चे घरों के आंगन में खटिया बिछा करती थी और पड़ोसी भी आकर बैठते थे। आंगन बटोरती मां की चुटिया पकड़कर बचपन मां की पीठ पर चढ़ता था। उस सुख का वर्णन कौन कर सकता है। मां के आनंद को और बच्चे के आनंद को!
काश, मैं फिर से अपनी मां के आंचल की छाया में अपने पुराने गांव के कच्चे घर में जन्म लेकर सो जाने का सुख पाता! वहां मैं होता और मेरे बाप के कच्चे घर में मां का आंचल होता!
डॉ. सतीश “बब्बा”
यह भी पढ़ें-