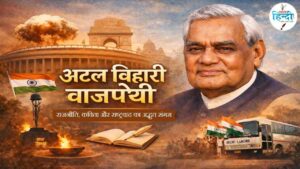कासे कहूँ दुखड़ा
Table of Contents
कासे कहूँ दुखड़ा
कासे कहूँ दुखड़ा: गति शील समाज के दो चिरंतन नियम हैं। सुनना और सुनाना, कहना और कहलवाना। समझना और समझाना। सुनना और सुनाना संवाद की स्थिति है। किसी की न सुनना और केवल अपनी सुनाना विवाद की स्थिति है। सुनना और सुनाना और फिर भी समस्या का समाधान न पाना, विषाद की स्थिति है। आज हमारे समाज का एक ख़ास वर्ग इसी तरह की समस्या से जूझ रहा है। वैसे यह वर्ग अपनी मुखरता के लिए प्रसिद्ध है। कबीर का यह दोहा विशेष रूप से इसी वर्ग के लिए कहा गया है-
रहिमन जिह्वा बावरी, कहत आकास-पाताल
आप कहतु भीतर गई, जूती खात कपाल।
इस स्प्ष्ट चेतावनी के बाद भी विडंबना तो देखो, इस वर्ग की शिकायतों का पिटारा कभी बंद ही नहीं होता।
‘हरि अनंत हरि कथा अनंता’
सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं भी इसी वर्ग से हूँ। हमेशा एक ही गाना:-
दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी।
अरे भाई! इसी सजनी से कह दे न। वैसे भी न तो यह बिना कहे रहने वाली है, न ही वह बिना सुने टलने वाली है। असल में दुखड़ा तो केवल सहानुभूति बटोरने का, अपनी तरफ़ ध्यानाकर्षण का एक सदियों पुराना और कारगर हथकंडा है। तो दुखियारी सजनी कवर्ग से लेकर श, से, ह तक की सारी कथा दूसरी सजनी को सुनाती है और साथ ही ताकीद करती है, “देख बहना, के वल तुझे ही बता रही हूँ और किसी से मत कहना। तुझे मेरी क़सम है।” सुनने वाली इतनी निष्ठा से गोपनीयता की क़सम खाती है कि भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा भी इसके सामने फ्यूज हो जाती है और अब विरोध का सौंदर्य देखिए।
सुनाने वाली सजनी के पीठ फेरते ही सुनने वाली सजनी तीसरी सजनी के पास पहुँचती है। मंथरा वाले स्टाइल में कहती है, “देख बहना, अमुक की बात बता रही हूँ, बस अपने तक ही रखना।” प्राण जाए पर वचन न जाई, वाले अंदाज़ में तीसरी सजनी वचन देती है और शाम को जब उसका सजन घर आता है तो उसे यह ख़बर मिर्च मसाला लगाकर बतौर स्नैक्स, चाय के साथ पेश करती है। सजन एक कान से सुनता है दूसरे कान से बाहर निकाल देता है और कुछ सार तत्त्व को बतौर हेडलाइन मन में रख लेता है। नतीजतन सुबह होते-होते यह परम गोपनीय बात मोहल्ले के हर न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज बन कर प्रसारित होती दिखाई देती है और शाम होते-होते सजनियाँ फिर गाती नज़र आतीं हैं-
दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी।
क्या करें, रोज़ नया दिन नया दुखड़ा। प्राचीनकाल में ऐसा नहीं होता था। इतिहास गवाह है कि सजनियाँ मन की विदा मन में ही छिपा लेतीं थीं। कुंती को याद करें। कर्ण के बारे में सबकुछ छिपा गईं। जब पांडु अपने निस्संतान होने का दुःख मना रहे थे, तब भी चुप रही, जबकि कौरवों की वंशोत्पत्ति से सुपरिचित थीं। लेकिन कुंती बोलने वालों की कैटेगरी में नहीं आती थीं, हो चुप रहीं। बात सामने आती भी नहीं, लेकिन होनी प्रबल होती है। ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई।
महाभारत के युद्ध के बाद सभी बचे-खुचे लोग अपने मृत सम्बंधियों का तर्पण करने पहुँचे। पांडव भी आए। धर्म राज और अन्य पांडवों ने तर्पण क्रिया प्रारंभ की कि माता कुंती बोलीं, “पुत्र ठहरो। कर्ण का भी तर्पण करो।” पांच जोड़ी विस्मित आंखें मातुश्री के मुखारविंद पर चस्पां हो गईं। कुंती निर्विकार भाव से बोलीं, “कर्ण तुम्हारे ज्येष्ठ थे। तुम्हारे बड़े भ्राता थे।” युधिष्ठिर ने मन ही मन माथा पीट लिया। आदरणीया जननी! ये बात पहले बता देतीं तो किसी के तर्पण की नौबत ही नहीं आती। भ्राताश्री कर्ण के बिना तो दुर्योधन और सारी चांडाल चौकड़ी की वैसे ही टांय-टांय फि्स्स हो जाती। पूरी जवानी वनों में भटक-भटक कर काट दी।
हर किसी से ऐसी की तैसी करवा ली और अब जब सारी रामायण ख़त्म हो गई, तो माताजी पर सच बोलने का शौक सवार हो गया। प्रश्र भरी दृष्टि से जननी की ओर निहारा। कुंती बोलीं, “मैं ने कृष्ण को बताया था।” कृष्ण बोले, “मैं ने भैया कर्ण को समझाया था पर बंदा टस से मस नहीं हुआ। ऐसा चिपका दुर्योधन से कि अंत तक चिपका ही रहा।” भीम बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किए थे।
अर्जुन अपराध-बोध से भरे थे। नकुल सहदेव किंकर्तव्यविमूढ़ से खड़े थे। आख़िर कार युधिष्ठिर ने खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत चरितार्थ करते हुए, माताश्री की गलती का बदला पूरी नारी जाति से लिया। फौरन श्राप देने की मुद्रा में बोले, “अब से नारी जाति के पेट में कोई बात नहीं पचेगी।” धर्म राज का श्राप था सच तो होना ही था, हो हुआ और तभी से क्यह नारी जाति एक्सट्रा वोकल हो गई। हर गली-गली दुःख बड़ा सुनाने लगी। नतीजा यह हुआ कि सुनने वाले कम पड़ गए और फिर वही समस्या पैदा हो गई:
कासे कहों मैं दुखड़ा?
वैसे इसी संदर्भ में एक और नारी चरित्र अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह है राक्षस राज रावण की इकलौती प्रिय बहन शूर्पणखा का। यह मुखरा नारी, बहुत सही निर्णय क्षमता वाली, बिंदास बुद्धिमती युवती थी। श्रृंगार, रूप सज्जा, प्रसाधन में निपुण। उसके सूप के समान सुंदर नाखून थे जिन्हें वह नित्य नई नेल आर्ट से सजाती थी। दंडकारण्य में इतराती इठलाती विचरती थी। एक दिन अचानक ही उसने श्रीराम लक्ष्मण को देखा। फौरन ही उसे श्रीराम से प्रथम दृष्टि का प्यार हो गया और उसने फौरन ही श्रीराम को प्रपोज कर दिया।
तुम सम पुरुष, न मो सम नारी,
यह संजोग विधि रचा विचारि।
लेकिन राम ने विधाता के इस दुर्लभ संयोग को सिरे से नकार दिया। “हे सुंदरी। मैं विवाहित हूँ। अतः तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं।” और फिर उन्होंने उसका परिचय सीता जी से कराया। वैसे यहाँ एक बात मुझे हैरान करती है। उस समय बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। स्वयं महाराज दशरथ ने तीन-तीन विवाह किए थे। श्रीराम भी उनके नक्शे-कदम पर चल सकते थे। लेकिन राम तो राम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक पत्नीव्रती थे। सो बिना लाग-लपेट के अपनी बात शूर्पणखा को समझाई और उसे चलता किया।
हाँ, उसकी बात को ध्यान में रखते हुए, उसे लक्ष्मण का नाम सजेस्ट कर दिया। शूर्पणखा ने भी मान लिया। कुछ भी तो ग़लत नहीं किया। एक जगह बात न बनने पर आदमी दूसरी जगह ट्राई करता ही है। वैसे लक्ष्मण को देखते ही उसे यह तो समझ आ गया था कि यह छोटा है तो एटीट्यूड वाला। बड़े भाई जैसा सोबर तो कतई नहीं है। लेकिन सुंदरता में उससे बीस ही है। प्रणय की मारी, बेचारी पहुँच गई लक्ष्मण के पास। वैसे उसका प्रोफाइल भी तो बहुत हाई फाई था। सुरुचि संपन्ना, रूपवती युवती थी। दंडकारण्य की शासिका थी। रावण की इकलौती प्रिय बहन थी। उसे अनदेखा करना इतना आसान भी नहीं था।
लेकिन लखनलाल तो बिना उसकी बात सुने, छुरी लेकर, उसके नाक-कान के पीछे पड़ गए। बेचारी ने बड़ी मुश्किल से भाग कर जान बचाई। लेकिन चुप न रही। सीधे भ्राताश्री रावण के दरबार में पहुँची और अपनी असफल प्रेमगाथा, रो-रोकर, करूण स्वर में सुनाई। रावण की बीसों भुजाएँ फड़क उठीं। नेत्र क्रोध से रक्तिम हो गए और दसों सिरों का पारा थर्मामीटर तोड़ सातवें आसमान पर पहुँच गया। जिसके भय से तीनों लोकों की धिग्गी बंध जाती है, उसकी बहन का भीषण अपमान और वह भी दो वनवासी छोकरों ने कर दिया। बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। फौरन सभा स्थगित कर, धटना-स्थल की ओर कूच किया।
इधर शूर्पणखा राजवैद्य से अपनी नाक का ट्रीटमेंट करवाती हुई सोच रही थी, अब भ्राताश्री गए हैं, दोनों में से एक को तो उठा ही लाएंगे और उसकी प्रेम-कहानी का सुखांत होगा। लेकिन दुखियारी के भाग में सुख कहाँ? भाईसाहब तो राम-लक्ष्मण दोनों को झांसा दे सीता को ही उठा लाए और अपनी एक तरफा प्रेम कहानी शुरु कर दी। अब शूर्पणखा तो रोएगी ही:-
दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी।
कहने का सारांश है कि न कहने वाला भी दुखी, कहने वाला भी दुखी। दुःख दोनों ही स्थितियों में कॉमन फैक्टर है। तो अब किया क्या जाए? वैसे एक बात मुझे आज ही समझ आई कि जैसे एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, वैसे ही एक असफल नारी के पीछे एक पुरूष का हाथ होता है। यह दूसरी बात है कि इस पुरूष की प्रेरणा स्रोत, उसकी मां, भाभी, बहन जैसी कोई नारी ही होती है।
जिसे हम दोस्त कहते थे, वही निकला दुश्मन हमारा।
तुलसी दास जी ने तो बहुत पहले ही इस बात पर मोहर लगा दी थी।
नारी न मोहे नारी के रूपा।
बात कड़वी है, मगर है सच्ची। हाँ, अब एकाध पर्सेंट अपवाद भी मिल सकता है। वैसे निन्यानवें प्रतिशतं तो यही सही है कि जहाँ एक नारी ने दूसरी को सुखी देखा, वहीं उसका कॉम्प्लेक्स सिर उठाता है। मेरे पड़ोस में एक सभ्य, सुशील, सबला महिला रहतीं हैं। उनका पति घर बाहर दोनों संभालता है। आदर्श पति है। सुबह खाना बना कर आफिस जाता है, शाम को फिर आकर खाना बनाता है। पत्नी शापिंग, किटी पार्टी वगैरह में व्यस्त रहतीं हैं। उनका जीवन स्मूथली चल रहा है।
‘मियाँ बीवी राजी वाला’ अंदाज़ है जीने का, लेकिन मोहल्ले की अबला काजियों को, नारी का यह सशक्तिकरण पसंद नहीं आता। मौका मिलते ही सबला निंदापुराण शुरू हो जाता है। “अजी कैसी बेशर्म है। बेचारे पति को गुलाम बना रखा है।” कुछ सती सावित्री टाइप कहती हैं, “पति तो भगवान् होता है। पाप लगेगा, अरे भई, भगवान से डरो।” निंदा-पुराण का समापन कर जब ये घर जाती हैं, तो इनका तथाकथित भगवान् या बेचारा पति इनकी दुर्गति कर देता है। फिर ये अपना दुखड़ा ज़माने भर को सुनाती फिरती हैं।
स्थिति सचमुच शोचनीय है। इन अबलाओं का मन पसंद टारगेट होती हैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखीआत्मनिर्भर युवतियाँ। उनकी सारी योग्यता, विद्वता, उपलब्धि और परिश्रम इनके लिए कोई महत्त्व नहीं रखता। उसे एक सिरे से नकारते हुए, ये उनकी निंदा में जी जान से लग जाती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसकी शुरुआत हमेशा इनकी अपनी बहू बेटियों के महिमा गायन से होती है, लेकिन बीच में ही विषयांतर हो जाने से, इस आलोचना का अंत एक दूसरे की बहू-बेटियों की छीछालेदर से होता है। नतीजा, ये एक दूसरे को अनेक शुभकामनाओं से नवाजती हुई, परम दुखी हो जाती हैं।
सचमुच इनके दुःख का कोई ओर-छोर ही नहीं है। कहीं से भी शुरू हों, अंत वही होता है। क्या कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है, बशर्ते ये एकजुट हो जाएँ। एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ अपनी टांग संभालें। कहें कम, सहें कम, सुनना-सुनाना, छोड़ करना सीखें। अपने वर्ग की उपलब्धियों पर गर्वित हों, हर्षित हों। उन्हें प्रोत्साहित करें। उनके मार्ग की हर बाधा दूर करें। संकीर्णता और हीनता के दायरों से मुक्ति पाएँ। तब दुखवा मैं कासे कहूँ, वाला मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। न होगा दुःख, न होगा उसका बखान। चैन की बंशी बजेगी और राधा हर टेढ़े आंगन में भी, बिना नौ मन तेल के भी नाच लेगी।
मेरी पीर न जाने कोय
आज बहुत दिनों के बाद सुबह की सैर पर निकला। सोचा, प्रकृति के दर्शन होंगे। प्रकृति का नजा़रा तो देखा ही, साथ ही साथ देश की पीर का दृश्य भी देख आया। सुबह-सुबहप्राकृतिक परिवेश में नित्यक्रिया से निवृत होता देश का वर्तमान और भविष्य, कचरे के ढेर पर मुंह मारता देश का पशुधन, रोज़ लगती और रोज़ उखाड़ कर, बेची जाती रेलिंगो के सहारे, आजीविका अर्जित करते, ग़रीबी रेखा पर खड़े देश के जन-गण की पीड़ा से देख, मन अधीर हो गया। सचमुच, कितनी पीर है देश में और हमें इसका पता ही नहीं था। हर कोई रो रहा है।
चहुं दिसि चीखों-पुकार मची है। ‘ मैं तो दरद दीवाना, मेरी पीर न जाने कोय। सचमुच बड़ी शर्म आई, अपनी इस गलफ़त पर। चुल्लू भर पानी तलाश ही रहा था कि एक मैले-कुचैले नौनिहाल ने आकर मेरा दामन थाम लिया और गुहार लगाई, “अंकल, कुछ दे न। सूबू से कुछ नईं खाया। ऐ, दे ना, अंकल।” मेरा मन भाव विह्वल हो उठा। कितनी आत्मीयता भरी है मेरे देश में। विवेकानंद जी इस आत्मीयता के बलबूते पर ही, भाषण देने से पहले ही, शिकागो धर्मसम्मेलन में छा गए थे। हम हर किसी को अपना कहते आए हैं, मानते कितना हैं, यह अलग विषय है।
पहले हम बाबा, भैया, माताजी, अम्मा आदि सम्बोधन करते थे, अब अंग्रेज़ी फैशन के चलते सारीआत्मीयता अंकल-आंटी में समा गई है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट वहीं है। मैंआत्मीयता के सैलाब में बहा जा रहा था कि भतीजेनुमा पीर ने ज़ोर से कुर्ता खींचा, और दांत निपोर कर बोला, “ऐ अंकल, दे न” मैंने सोचा कि क्यों न ताजा-ताजा पैदा हुए ई आत्मग्लानि से छुटकारा पाया जाए, फौरन उसे पांच का नोट थमाया और आगे बढ़ा, लेकिन बढ़ नहीं पाया। देश की पीर ने रास्ता रोक लिया। दो-चार मैली-कुचैली पीरों ने मुझे घेर लिया और उन पीड़ाओं की जननी सड़क की पटरी पर बैठी जुओं से भरा सिर खुजा रही थी।
बड़ी मुश्किल से उनसे छुटकारा पाया। घर पहुँचा तो सोचा आज श्रीमती जी से इसी विषय पर बात करेंगे। ‘गर्म चाय और देश की पीर’ कितना यूनीक और बौद्धिकता भरा विषय है। भाव और बुद्धि का सुपर कॉम्बीनेशन। आकर कुर्सी पर बैठा ही था कि श्रीमती जी आईं। अकेले नहीं, अपनी पीर भी साथ लाईं थीं। उनकी पीर बड़ी जैनुईन थी। बोलीं, “एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गई है महारानी गाँव में। कह रही थी कि माँ बीमार है। झूठी कहीं की। अब खटो दिनभर चूल्हे में।” और वे सोफे पर पसर गईं।
मैं फौरन देश की पीर भूल गया। श्रीमती जी, महारानी की माँ की, और इस वज़ह से ख़ुद को होने वाली पीर का एहसास मुझे बड़ी शिद्दत से होने लगा। अपनी उपेक्षा होती देखकर देश की पीर मुझे शिकायत भरी नजरों से देखने लगी। मैं क्या करता, कह दिया उसे, “अरे भई, यहाँ अपनी ही पीर से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो तेरी पीर कैसे देखूं।”
और अब तो आलम यह है कि मर्ज़ बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। और भईया, हम तो दवा क्या, दुआ करने से भी बाज नहीं आए। हर समय दुआ करने की सुविधा रहे, यह सोचकर भगवान जी का अपहरण कर उसे भी मंदिर से घर में ले आए। जकड़ दिया उसे भी छूआछूत, ऊंच-नीच, जाति-पांति के बंधनों में। और इस क़दर जकड़ा कि वह भी पुकार उठा, “मेरी पीर न जाने कोय।”
अब तो बंधु, यह पीर अपार अनंत होती जा रही है। सुरसा का मुंह, हनुमान की पूंछ, राजनीति की मूंछ, जो सभी इसके सामने बौनी पड़ गई हैं। पीर का परबत ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा है, और अब तो दुष्यंत कुमार जैसे जांबाजों ने भी उसमें से गंगा निकलने की आस छोड़ दी है और गंगा निकले भी तो कैसे? उसके निकालने का बजट तो प्रसाद की भांति ऊपर से नीचे तक, यहाँ से वहाँ तक, कभी कमीशन, कभी चंदे, कभी प्रबंधन, कभी क्षतिपूर्ति, कभी मुनाफाखोरी के नाम पर कहाँ से कहाँ तक बंट चुका है।
कितनी भी तपस्या कर लें भगीरथ, अब सगरपुत्रों की आत्माओं का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, चाहें तो इस प्रजातंत्र की मरूभूमि में भटक-भटक कर, जंतर-मंतर पर, रेल की पटरियों पर, संसद से सड़क तक कहीं भी, हर गली कूचे में स्वर बुलंद कर सकती हैं, “मेरो दर्द न जाने कोय”। पर होगा कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज़्यादा आंदोलन-अनशन कर लेंगी। नारे लगा लेंगी शासन की लाठियाँ खा लेंगी, टी. आर ।पी बढ़ा लेंगी, सुर्खियों में छा लेंगी, पर नतीजा वही होगा शून्य बटा सन्नाटा।
एक पीर और भी खड़ी है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, वाले स्टाइल की। यह युगों-युगों की पीर है। मीरा बाईं ने इसकी ज़ोर-शोर से पुष्टि की, हे थी, “मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दरद न जाने कोय।” जब सब जानती हो तो काहे को पुकार रही हो मीरा रानी? तेरी पीर तो न उस युग में किसी ने जानी थी और न ही यह युग जानने को क्या मानने को भी तैयार हैं। अब तो “लव जिहाद” का और नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। तेरा चुप होना ही ठीक रहेगा। तू भले ही कितना शोर मचा ले, आसमान में उड़ जा, पाताल फोड़ दे, अपनी शक्ति सामर्थ्य के परचम जगह-जगह गाड़ दें, पर हमारे अंधे गूंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यिर वाले समाज के अहं पर जूं तक नहीं रेंगेगी।
तू भी बहुत-सी झूठी संवेदनाएँ बटोर लेगी, लोग मोमबत्तियाँ जला लेंगे, नारे लगा लेंगे, विपक्ष की छीछालेदर कर लेंगे, फिर तू भी हाशिए से रपट जाएगी। खो जाएगी। यह समाज तुझे ज़हर देने से बाज नहीं आएगा। तुझे पैदा ही नहीं होने देगा। और अगर पैदा हो गई तो तुझे ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि तू पैदा ही क्यों हुई। मत सोच कोई तुझे तेरी पीर से निजात दिलाने आएगा। तुझे ख़ुद ही रास्ता ढूँढना होगा।
लेकिन हम सभ्य होने का दम भरते हैं। और अब तो सभ्यता को भी पीर का बढ़ता साम्राज्य देख पीड़ा होने लगी है। अरे भई, कुछ तो लाज रख लो सभ्यता की। माना कि हमारी कथनी और करनी में छत्तीस का आंकड़ा है, पर कभी तो दोनों को एक होने दो। देश की महान परंपरा की विरासत संभालने का दावा करते हो, कभी तो महानता की ओर बढ़ों। ‘मैं मैं’ की बकरी भाषा छोड़, ‘हम हम’ की सिंह गर्जना करो। आदर्शों का भार कब तक ढोते रहोगे, कभी तो व्यवहार के धरातल पर उतरो। अपने से परे देखो। अधिकार से पहले कर्त्तव्य निभाना सीखो। तभी तो पीर दूर होगी सबकी और कबीर मग्नमन गा पाएंगे:-
कबिरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर।
जो पर पीर न जानहिं, सो काफ़िर बेपीर।
वीणा गुप्त
नई दिल्ली
यह भी पढ़ें-